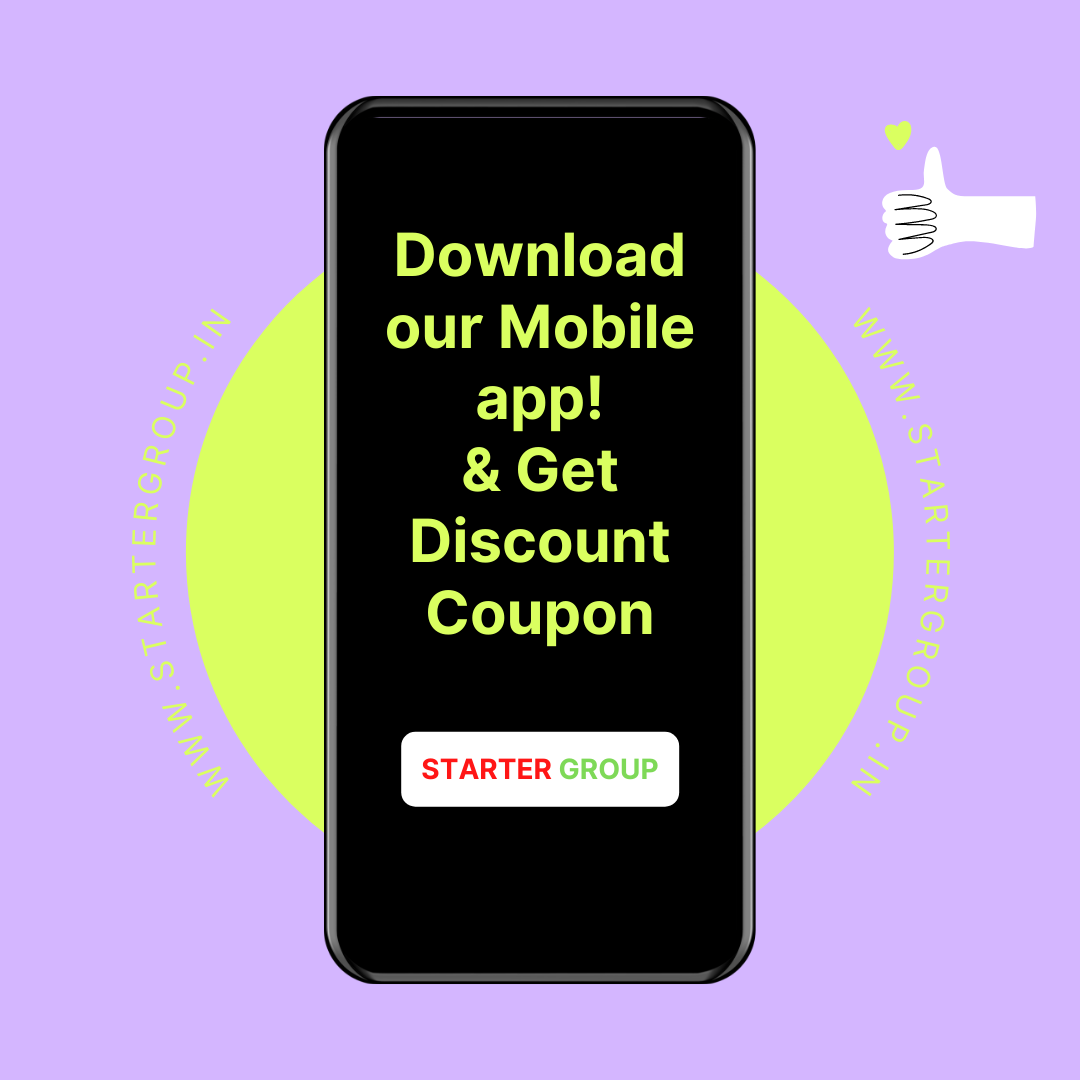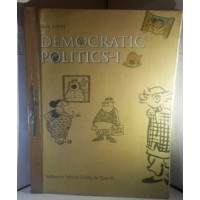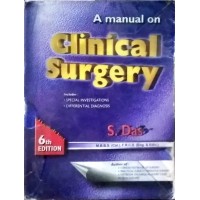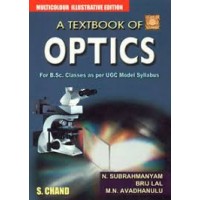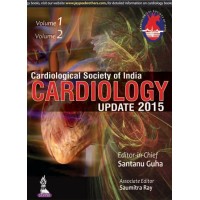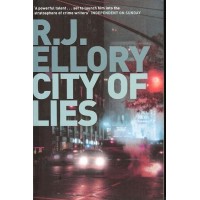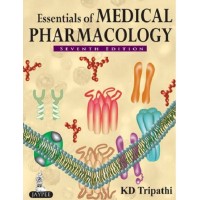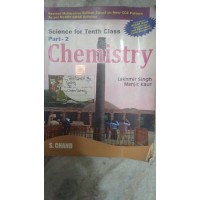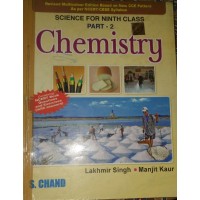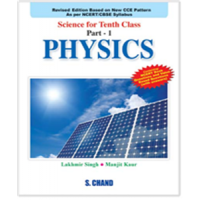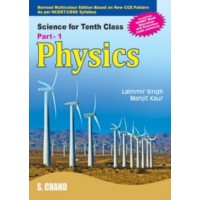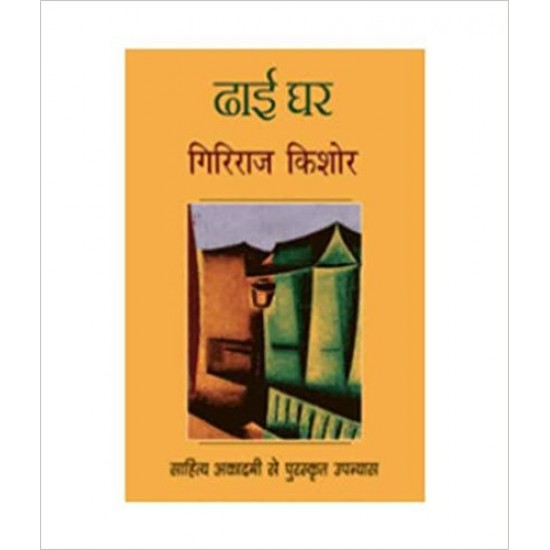
-60 %
Out Of Stock
Dhai Ghar (Hindi) Hardcover – 1 Jan 2001 by Giriraj Kishore
प्रख्यात उपन्यासकार गिरिराज किशोर के उपन्यास ‘ढाई घर’ में ऐसे अनेक रंग, रेखायें, चरित्र और परिवेश के स्वर हैं जो नये समाज और उसकी धड़कन को बिल्कुल नयी भंगिमा के साथ प्रस्तुत करते हैं।
यह उपन्यास क्यों ?
जब मेरे सामने बिशन भाई का यह प्रस्ताव आया कि मैं ‘जुगलबन्दी’ जैसा कि उपन्यास लिखूँ तो ऐसा नहीं कि मैं यह न समझा हूँ कि इस वाक्य में व्यंजना क्या है। लेकिन न जाने कैसे वह वाक्य ज्यूँ का त्यूँ मेरे दिमाग़ में उतर गया। मेरे अन्तर्मन में यह प्रश्न उठ खड़ा हुआ-क्या वास्तव में ‘जुगलबन्दी’ में सब कुछ कहा जा चुका ? उसके अलावा कुछ नहीं कहना ? लगभग ऐसा ही प्रश्न तब भी उठा था जब ‘लोग’ लिख लेने के बाद ‘जुगलबन्दी’ लिखना ठीक होगा या नहीं ? तब इतने-से उत्तर से ही काम चल गया था कि ‘लोग’ ‘जुगलबन्दी’ नहीं है। ‘जुगलबन्दी’ का लिखा जाना अभी बाकी है। वास्तव में ‘जुगलबन्दी’ ‘लोग’ था भी नहीं। इस बार यह सवाल कुछ ज़्यादा शिद्दत के साथ, कई रंगों में सामने आया। आखिर उस वातावरण पर कब तक लिखते रहोगे ? क्या तुम्हारे पास लिखने को और कुछ नहीं ?
मेरे कुछ मित्रों ने यह भी कहा कि अगर ऐसा ही है तो ‘जुगलबन्दी’ का दूसरा भाग क्यों नहीं लिख लेते ? पर मैं सच कहूँ कि इन सवालों ने मुझे अपने आपको और ज़्यादा टटोलने का मौका दिया। मुझे यही लगा कि अभी तो वातावरण और समाज के ऐसे बहुत से पक्ष बाकी हैं जिनका, नये बनते या बने समाज को समझने के लिए, सामने आना ज़रूरी है। उन बातों को मैं नहीं कहूँगा तो शायद मेरी पीढ़ी का कोई और लेखक न कहे। जाना हुआ जीवन कई बार अपने आपको छोटे-छोटे अन्तरालों के बाद टुकड़ों-टुकड़ों में खोलता चलता है और लेखक के लिए चुनौती बनता जाता है।
लेखक को उस चुनौती का खुले दिलो-दिमाग़ के साथ सामना करना पड़ता है। क्योंकि जब तक लेखक उस सबको को कह नहीं लेता तब तक वह अपने आपको उस रचनात्मक दबाव से मुक्ति नहीं दिला पाता। लेखक अपने अनुभव, दु:खों ओर सुखों को अपने पाठकों के साथ बाँटता है, उनसे हिस्सेदारी करता है, उसके अलावा उन्हें देने के लिए लेखक के पास कुछ और है ही नहीं। उसकी अन्तरंग से अन्तरंग बातों में उसके पाठक ही हिस्सेदार होते हैं। कई बार वे बातें स्वीकार्य होती हैं, कई बार नहीं होतीं और कई बार स्वीकृति या अस्वीकृति में ही कई दशक लग जाते हैं।
जिस माहौल में, जिस संस्कृति और जिन स्थितियों से उपजे अनेक छोटे-बड़े पात्रों को, उनकी कुंठाओं, उनके छोटेपन या बड़प्पन को देखा, उनका एक बहुत बड़ा हिस्सा मेरे स्मृति कोष में अभी बाकी है। जब यह बात मेरे सामने आयी तो जैसे सब कुछ खुलता और फैलता चला गया। मेरे पास यही एक रास्ता रह गया था कि मैं उस माहौल को पुन: जिऊँ और उस पर लिखूँ। कई बार लेखक अपनी मुक्ति के लिए भी लिखता है और अपने नये-पुराने समाज की पहचान के लिए भी। इसके दोनों ही पक्ष होते हैं-नुकसान भी और सार्थकता भी। साहित्य में होने वाला सबसे बड़ा नुकसान रचनाकार की रचना का अस्वीकार ही है। लेखक को उसके लिए हर समय तैयार रहना पड़ता है। क्योंकि रचना को सार्थक बनाना उसके पाठकों के हाथ में है। इस बारे में लेखक स्वयं कुछ नहीं कर सकता।
एक बात और है। मुझे समाज और मनुष्य, मनुष्य और मनुष्य तथा व्यक्ति और प्रतिष्ठान के बदलते रिश्ते हमेशा से आकर्षित करते रहे हैं। कहानी हो या नाटक या उपन्यास या लेख, मैं इन बदलते रिश्तों निरन्तर सामने लाने की कोशिश करता रहा हूँ। मेरी इच्छा हमेशा उन बदलते रिश्तों का गायक बने रहने की रही है।
एक वक़्त और एक समाज में जो कुछ बदलता है वह अगले समाज में बनने वाले रिश्तों का आधार होता है। ‘कोशिश’ शब्द का प्रयोग करने के पीछे मेरा मात्र मतलब कोशिश ही है उपलब्धि नहीं। लेखन-प्रयत्न-जीवी है। उपलब्धियों का क्षेत्र विज्ञान है, व्यवसाय है, राजनीति आदि हैं। साहित्य तो बहुत बाद में आता है। यहाँ असफलताएँ ही सफलता का रास्ता दिखाती हैं। वैसे तो ऐसे भी लेखक हैं जो अपनी हर कोशिश की उपलब्धि में बदलने का प्रयत्न करते हैं। एक रचना लिखकर वे तब तक उसका प्रचार करते हैं जब तक उसे उपलब्धि न मान लिया जाये। लेकिन यह कितने दिन चल पाता है। लेखन तो एक आवा है। उसमें हजारों मिट्टी के कच्चे दीये लगते हैं तो कुछ प्रथम कोटि के बनकर निकलते हैं, कुछ अधपके, कुछ टूटे हुए। खाली या अधपके आवे से यह उम्मीद करना ही हर रचना श्रेष्ठतम बनकर निकले असंभव को साधने का स्वप्न देखने की तरह है।
मैं यह भी जानता हूँ कि पुनरावृत्ति चाहे माहौल की हो या किसी समाज की या पात्रों की, पाठक उसे बड़ी मुश्किल से स्वीकार करता है। लेकिन वृत्ति, आवृत्ति, पुनरावृत्ति यदि ये सब किसी समाज को संगठित करके पेश करने और उसके बारे में समझदारी बनाने में सहायक होती हैं तो लेखक के लिए उस खतरे को उठाना ज़रूरी हो जाता है।
अगर वह ऐसा नहीं करता तो अपने लेखकीय दायित्व पर वह स्वयं ही प्रश्न चिह्न लगाता है। किसी और के सामने उत्तरदायी होता ही है। मेरे लिए उपन्यास या कहानी अब मनोरंजन के माध्यम नहीं। शायद यही कारण है कि मेरी रचनाएँ लेखक के साथ-साथ पाठक पर भी एक तरह का दबाव बनाती हैं। दबाव सहज स्वीकार्य नहीं होता, चाहे वह किसी भी तरह का दबाव क्यों न हो। इसीलिए वे उतनी जन-व्यापी नहीं हो पातीं। मैं उपन्यास को एक समाजशास्त्री अध्ययन भी मानता हूँ-अनेक प्रकार के संबंधों को, जो रहे हैं, या हैं या आगे बनेंगे, व्याख्यायित करने वाले मानवीय समीकरण। मेरी दृष्टि में उपन्यास और कहानियाँ, बल्कि नाटक भी, जीवन के प्रति वैज्ञानिक और अर्ध-वैज्ञानिक दृष्टिकोण बनाने में मदद करते हैं और उन्हें ऐसा करना चाहिए। यशपाल की रचनाएँ काफ़ी हद तक इस दृष्टि से महत्त्वपूर्ण हैं। जो हम आज लिख रहे हैं वही जीवन के प्रति दृष्टिकोण निर्धारित करने में आने वाली पीढ़ी की मदद करेगा। न सही युग-प्रवर्तक साहित्य के रूप में-खाद का योगदान भी कम नहीं होता।
मुझे यह उपन्यास एक लेखकीय दायित्व के निर्वाह की तरह लगा। ये सब बातें आत्म-औचित्य प्रतिपादन की तरह भी मालूम पड़ सकती हैं परन्तु उससे विशेष अन्तर नहीं पड़ता, क्योंकि लेखक जीवन भर यही तो करता है। कभी अपने लिए, कभी समाज और जीवन की दृष्टि से, अपने आपको रात-दिन धुनकर उन निष्कर्षों या तथ्यों तक पहुँचता है जो उसके अस्तित्व के होने को सही ठहराते हैं।
यह उपन्यास नितान्त किस्सागोई है। कभी-कभी लग सकता है कि तारतम्य गड़बड़ा गया। पर ऐसा है नहीं। सूत्र अपने आप चटकते और एक-दूसरे से जुड़ते रहते हैं। यह एक लम्बी उठान वाली, टूटी-टूटी कथा है जो एक समाज से दूसरे समाज में बदलते संबंधों को रेखांकित करती है।
मैं कह नहीं सकता कि इस उपन्यास के बारे में बिशन भाई की क्या प्रतिक्रिया होगी। लेकिन मैं यह जानता हूँ कि उनके इतना कहने मात्र ने मेरी स्मृति-कुण्ललिनी जाग्रत कर दी। वरना पता नहीं कब और किस रूप में वे स्मृतियाँ सामने आतीं ! आती भी या नहीं ! हो सकता है मैं उनसे, वे मुझसे अनजान ही बने रहते। बिशन जी ने मेरी एक और सहायता भी की, कई तथ्यात्मक प्रतिक्रियाओं और स्थितियों की जानकारी देकर मुझे सुधार करने का अवसर दिया।
इस उपन्यास के नाम के बारे में भी मैं काफी शशोपंज में था। पहले मैंने इसका नाम ‘रघुबर सब जानता है’ रखा, फिर ‘घोड़े’ रखने की सोची, लेकिन अन्त में मुझे ‘ढाई घर’ ही ठीक लगा। ‘ढाई घर’ और ‘घोड़े’ का वैसे भी गहरा संबंध है। शतरंज का घोड़ा आगे-पीछे सब घर चलता है। नाम के लिए राजेन्द्र को धन्यवाद देना शायद ज़रूरी है।
मेरे कुछ मित्रों ने यह भी कहा कि अगर ऐसा ही है तो ‘जुगलबन्दी’ का दूसरा भाग क्यों नहीं लिख लेते ? पर मैं सच कहूँ कि इन सवालों ने मुझे अपने आपको और ज़्यादा टटोलने का मौका दिया। मुझे यही लगा कि अभी तो वातावरण और समाज के ऐसे बहुत से पक्ष बाकी हैं जिनका, नये बनते या बने समाज को समझने के लिए, सामने आना ज़रूरी है। उन बातों को मैं नहीं कहूँगा तो शायद मेरी पीढ़ी का कोई और लेखक न कहे। जाना हुआ जीवन कई बार अपने आपको छोटे-छोटे अन्तरालों के बाद टुकड़ों-टुकड़ों में खोलता चलता है और लेखक के लिए चुनौती बनता जाता है।
लेखक को उस चुनौती का खुले दिलो-दिमाग़ के साथ सामना करना पड़ता है। क्योंकि जब तक लेखक उस सबको को कह नहीं लेता तब तक वह अपने आपको उस रचनात्मक दबाव से मुक्ति नहीं दिला पाता। लेखक अपने अनुभव, दु:खों ओर सुखों को अपने पाठकों के साथ बाँटता है, उनसे हिस्सेदारी करता है, उसके अलावा उन्हें देने के लिए लेखक के पास कुछ और है ही नहीं। उसकी अन्तरंग से अन्तरंग बातों में उसके पाठक ही हिस्सेदार होते हैं। कई बार वे बातें स्वीकार्य होती हैं, कई बार नहीं होतीं और कई बार स्वीकृति या अस्वीकृति में ही कई दशक लग जाते हैं।
जिस माहौल में, जिस संस्कृति और जिन स्थितियों से उपजे अनेक छोटे-बड़े पात्रों को, उनकी कुंठाओं, उनके छोटेपन या बड़प्पन को देखा, उनका एक बहुत बड़ा हिस्सा मेरे स्मृति कोष में अभी बाकी है। जब यह बात मेरे सामने आयी तो जैसे सब कुछ खुलता और फैलता चला गया। मेरे पास यही एक रास्ता रह गया था कि मैं उस माहौल को पुन: जिऊँ और उस पर लिखूँ। कई बार लेखक अपनी मुक्ति के लिए भी लिखता है और अपने नये-पुराने समाज की पहचान के लिए भी। इसके दोनों ही पक्ष होते हैं-नुकसान भी और सार्थकता भी। साहित्य में होने वाला सबसे बड़ा नुकसान रचनाकार की रचना का अस्वीकार ही है। लेखक को उसके लिए हर समय तैयार रहना पड़ता है। क्योंकि रचना को सार्थक बनाना उसके पाठकों के हाथ में है। इस बारे में लेखक स्वयं कुछ नहीं कर सकता।
एक बात और है। मुझे समाज और मनुष्य, मनुष्य और मनुष्य तथा व्यक्ति और प्रतिष्ठान के बदलते रिश्ते हमेशा से आकर्षित करते रहे हैं। कहानी हो या नाटक या उपन्यास या लेख, मैं इन बदलते रिश्तों निरन्तर सामने लाने की कोशिश करता रहा हूँ। मेरी इच्छा हमेशा उन बदलते रिश्तों का गायक बने रहने की रही है।
एक वक़्त और एक समाज में जो कुछ बदलता है वह अगले समाज में बनने वाले रिश्तों का आधार होता है। ‘कोशिश’ शब्द का प्रयोग करने के पीछे मेरा मात्र मतलब कोशिश ही है उपलब्धि नहीं। लेखन-प्रयत्न-जीवी है। उपलब्धियों का क्षेत्र विज्ञान है, व्यवसाय है, राजनीति आदि हैं। साहित्य तो बहुत बाद में आता है। यहाँ असफलताएँ ही सफलता का रास्ता दिखाती हैं। वैसे तो ऐसे भी लेखक हैं जो अपनी हर कोशिश की उपलब्धि में बदलने का प्रयत्न करते हैं। एक रचना लिखकर वे तब तक उसका प्रचार करते हैं जब तक उसे उपलब्धि न मान लिया जाये। लेकिन यह कितने दिन चल पाता है। लेखन तो एक आवा है। उसमें हजारों मिट्टी के कच्चे दीये लगते हैं तो कुछ प्रथम कोटि के बनकर निकलते हैं, कुछ अधपके, कुछ टूटे हुए। खाली या अधपके आवे से यह उम्मीद करना ही हर रचना श्रेष्ठतम बनकर निकले असंभव को साधने का स्वप्न देखने की तरह है।
मैं यह भी जानता हूँ कि पुनरावृत्ति चाहे माहौल की हो या किसी समाज की या पात्रों की, पाठक उसे बड़ी मुश्किल से स्वीकार करता है। लेकिन वृत्ति, आवृत्ति, पुनरावृत्ति यदि ये सब किसी समाज को संगठित करके पेश करने और उसके बारे में समझदारी बनाने में सहायक होती हैं तो लेखक के लिए उस खतरे को उठाना ज़रूरी हो जाता है।
अगर वह ऐसा नहीं करता तो अपने लेखकीय दायित्व पर वह स्वयं ही प्रश्न चिह्न लगाता है। किसी और के सामने उत्तरदायी होता ही है। मेरे लिए उपन्यास या कहानी अब मनोरंजन के माध्यम नहीं। शायद यही कारण है कि मेरी रचनाएँ लेखक के साथ-साथ पाठक पर भी एक तरह का दबाव बनाती हैं। दबाव सहज स्वीकार्य नहीं होता, चाहे वह किसी भी तरह का दबाव क्यों न हो। इसीलिए वे उतनी जन-व्यापी नहीं हो पातीं। मैं उपन्यास को एक समाजशास्त्री अध्ययन भी मानता हूँ-अनेक प्रकार के संबंधों को, जो रहे हैं, या हैं या आगे बनेंगे, व्याख्यायित करने वाले मानवीय समीकरण। मेरी दृष्टि में उपन्यास और कहानियाँ, बल्कि नाटक भी, जीवन के प्रति वैज्ञानिक और अर्ध-वैज्ञानिक दृष्टिकोण बनाने में मदद करते हैं और उन्हें ऐसा करना चाहिए। यशपाल की रचनाएँ काफ़ी हद तक इस दृष्टि से महत्त्वपूर्ण हैं। जो हम आज लिख रहे हैं वही जीवन के प्रति दृष्टिकोण निर्धारित करने में आने वाली पीढ़ी की मदद करेगा। न सही युग-प्रवर्तक साहित्य के रूप में-खाद का योगदान भी कम नहीं होता।
मुझे यह उपन्यास एक लेखकीय दायित्व के निर्वाह की तरह लगा। ये सब बातें आत्म-औचित्य प्रतिपादन की तरह भी मालूम पड़ सकती हैं परन्तु उससे विशेष अन्तर नहीं पड़ता, क्योंकि लेखक जीवन भर यही तो करता है। कभी अपने लिए, कभी समाज और जीवन की दृष्टि से, अपने आपको रात-दिन धुनकर उन निष्कर्षों या तथ्यों तक पहुँचता है जो उसके अस्तित्व के होने को सही ठहराते हैं।
यह उपन्यास नितान्त किस्सागोई है। कभी-कभी लग सकता है कि तारतम्य गड़बड़ा गया। पर ऐसा है नहीं। सूत्र अपने आप चटकते और एक-दूसरे से जुड़ते रहते हैं। यह एक लम्बी उठान वाली, टूटी-टूटी कथा है जो एक समाज से दूसरे समाज में बदलते संबंधों को रेखांकित करती है।
मैं कह नहीं सकता कि इस उपन्यास के बारे में बिशन भाई की क्या प्रतिक्रिया होगी। लेकिन मैं यह जानता हूँ कि उनके इतना कहने मात्र ने मेरी स्मृति-कुण्ललिनी जाग्रत कर दी। वरना पता नहीं कब और किस रूप में वे स्मृतियाँ सामने आतीं ! आती भी या नहीं ! हो सकता है मैं उनसे, वे मुझसे अनजान ही बने रहते। बिशन जी ने मेरी एक और सहायता भी की, कई तथ्यात्मक प्रतिक्रियाओं और स्थितियों की जानकारी देकर मुझे सुधार करने का अवसर दिया।
इस उपन्यास के नाम के बारे में भी मैं काफी शशोपंज में था। पहले मैंने इसका नाम ‘रघुबर सब जानता है’ रखा, फिर ‘घोड़े’ रखने की सोची, लेकिन अन्त में मुझे ‘ढाई घर’ ही ठीक लगा। ‘ढाई घर’ और ‘घोड़े’ का वैसे भी गहरा संबंध है। शतरंज का घोड़ा आगे-पीछे सब घर चलता है। नाम के लिए राजेन्द्र को धन्यवाद देना शायद ज़रूरी है।
| Books Information | |
| Author Name | Giriraj Kishore |
| Condition of Book | Used |
Rs.150.00
Rs.375.00
Ex Tax: Rs.150.00
- Stock: Out Of Stock
- Model: sg810
Tags:
Giriraj Kishore